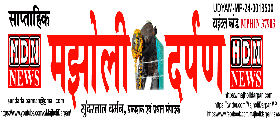भारतीय संविधान के निर्माता तथा आधुनिक भारत के मनु कहे जाने वाले दिवंगत बाबा साहब
डा. भीमराव अम्बेडकर के सतत् प्रवाभों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में ऐसा प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को देश की आबादी के एक विशेष वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इन्हें राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए विवेकपूर्ण संरक्षण, सहायता और निश्चयात्मक कार्य योजना के अन्तर्गत विशेषाधिकार की आवश्यकता महसूस की गई। फलतः संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए 15% व अनुसूचित जनजातियों के 7.5% उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई।
अंग्रेजों के जमाने में अनेक सामाजिक सुधार से सम्बन्धित आन्दोलनों के कारण ब्राह्मणवाद कुछ कमजोर होने लगा था। डा. अम्बेडकर जैसे मानवतावादी महापुरुष तथा मनस्वी महाचेता को संविधान बनाने का मौका ब्राह्मणवादियों ने कोई शौक से नहीं दिया था। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। यह कमीशन यह पता लगाना चाहता था कि भारत में कौन-कौन सी जातियाँ हैं जो पिछड़ी हैं और उनकी उन्नति के लिए क्या किया जाय? ब्राह्मणवादियों ने ‘जनेऊ पहनो आन्दोलन’ तथा ‘ऊँचा बनो अभियान’ (1928 से 1931 के बीच) चलाकर पिछड़ों को बहका दिया। वे बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह पर न चल सके और अपने विकास के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक आधार पर आरक्षण की माँग न कर सके। ब्राह्मणवादियों ने बड़ी चालाकी से ‘साइमन गो बैक’ का नारा लगवा कर अपना मनुवादी आरक्षण बनाये रखा।
*ब्रिटिश सरकार हिन्दू वर्णव्यवस्था के अन्तर्गत चतुर्थ वर्ण शूद्र को पददलित वर्ग/डिप्रेस्ड क्लास मानते थे और इसी आधार पर कुछ व्यवस्थाएं भी इस वर्ग के लिए आया।1925 बाबू रामचरनलाल निषाद एडवोकेट अपने सहयोगियों रामप्रसाद अहीर प्लीडर ,शिवदयाल चौरसिया,राजाराम कहार आदि के साथ मिलकर सभी शूद्रों/डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेवाओं व राजनीति में समान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।उन्होंने 1925 में बैकवर्ड फेडरेशन लीग के माध्यम से पूरे प्रदेश में सभाएं कर जागरण कर रहे थे।साइमन कमीशन जब लखनऊ आया तो इन लोगों ने उसका स्वागत किया तथा कमीशन के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखकर शूद्र वर्ण के लिए विशेष सहुलितों की माँग का ज्ञापन दिया।लोथियन कमेटी के समक्ष भी सभी के लिए एक समान वयस्क मताधिकार की मांग किया।बताते चलें कि अम्बेडकर जी बैकवर्ड फेडरेशन की दलील का जगह जगह प्रतिवाद करते रहे।उन्होंने कहा कि शूद्र वर्ण सछूत शुद्र(टचेबल डिप्रेस्ड) व अछूत शूद्र(अनटचेबल डिप्रेस्ड) में विभक्त है।अहीर व निषाद आदि के साथ भेदभाव नहीं होता है।यही पर आज की हिन्दू पिछड़ी जातियों के साथ धोखाधड़ी का खेल शुरू हो गया।जब अम्बेडकर मुम्बई प्रान्त से 1926 में एमएलसी नामित किये गए,उसी समय बाबू रामचरनलाल निषाद एडवोकेट संयुक्त प्रान्त के एमएलसी नामित किये गए।सछूत व अछूत की बात डॉ. अम्बेडकर द्वारा नहीं उठाई गई होती तो सभी शूद्रों को भारत सरकार अधिनियम-1935 में ही अधिकार मिल गया होता।सच अर्थों में अम्बेडकर जी सिर्फ अछूत दलितों की ही लड़ाई लड़ते थे।उन्होंने संगठन बनाये तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन व पार्टी बनाये तो शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी।*
ज्ञातव्य है कि उसी साइमन मकीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1932 ई. में जो गोलमेज कांफ्रेस के प्रकाश में पूना पैक्ट में महात्मा गाँधी और डा. अम्बेडकर में समझौता हुआ उसी समझौते के फलस्वरूप 1948 में संविधान का निर्माण करते समय बाबा साहब ने व्यवस्था बनाया, उसे अनुच्छेद-340 के नाम से जाना जाता है।जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया।यह अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार से सम्बंधित है,जो विधिक सलाहकार बीएन राव के द्वारा जुड़वाया गया।एक बात और बताना आवश्यक है कि भारत में सबसे पहले अदर बैकवर्ड क्लास का प्रयोग संविधान सभा की बैठक में 13 दिसम्बर,1946 को जवाहरलाल नेहरू ने किया।
अनुच्छेद-340 के तहत 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग बनाया गया,लेकिन इसकी सिफारिशें केन्द्र सरकार ने लागू न कर राज्यों के पल्ले में डाल दिया। जनता पार्टी की सरकार के समय 20 दिसम्बर,1978 को द्वितीय पिछड़ावर्ग आयोग का गठन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल(यादव) की अध्यक्षता में किया गया।जिसने 1 जनवरी 1979 को अपना कार्य शुरू किया।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक सचिव की भी नियुक्ति की गई। इस आयोग के गठन के बाद ही जुलाई 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व में एक लंगड़ी सरकार बनी। अगस्तं 1979 में पार्लियामेंट, भंग होने के बाद पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः प्रधान मंत्री बनीं। मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को पिछड़े वर्गों की जातियों की सूची में शामिल किया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 1980 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के समक्ष पेश की। इस रिपोर्ट को पेश करते समय श्री बी.पी. मंडल ने निम्न आशंका व्यक्त की थी।(द्वितीय पिछड़ावर्ग आयोग बीपी मण्डल की अध्यक्षता में गठित हुआ था,इसलिए इसे मण्डल कमीशन/मण्डल आयोग कहते हैं।)
“Apprehensions were rightly expressed before us that in case the report of my commission also meets the same fate as that of Kaka Kalelker’s commission, the legitimate hopes and aspirations of the socially and educationally backward classes, which constitute a bulk of population will be dashed to ground.”
इस प्रकार कमीशन के रिपोर्ट पेश करने में 2 वर्ष का समय लगा। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ ,विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। आंकड़े संकलित कराये गये-प्रश्नावालियों के द्वारा उत्तर प्राप्त किये गये। विविध राज्यों का दौरा किया गया। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सर्वे किये गये। सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्यों, केन्द्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों से सूचनायें माँगी गई। सातवीं लोक सभा के संसद सदस्यों, राज्य सभा के सदस्यों, राज्य के विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किये गये। इस प्रकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई। विधि विभाग तथा विविध मानक सामाजिक संस्थाओं से भी मदद ली गई। न्यायिक सद्घोषणाओं, संविधान तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की समस्त उद्घोषणाओं को भी दृष्टिपथ में रखा गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक संविधान सम्मत, न्यायसम्मत, वस्तु निष्ठ तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं अनुकूल सामाजिक न्याय का आधार है।
जब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई तब से लेकर 7 अगस्त, 1990 तक वह ठंडे बस्ते में बंद रही। यदि पंडित नेहरू ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को दबाये रखकर अपनी उच्च वर्णीय ब्राह्मणवादी मानसिकता को उजागर किया तो दिवंगत श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनके सुपुत्र श्रीमान् राजीव गांधी जी ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 7 अगस्त 1990 को जनता दल के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी की। अब मैं अपने प्रिय पाठकों को यह बतलाना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन की अनुशांसायें क्या हैं और पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसमें से क्या-क्या लागू करने की अधिसूचना जारी की थी?
*मण्डल आयोग की मूल सिफारिशें*
(13.1) ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पिछड़ा वर्गो का उत्थान, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन जैसी व्यापक राष्ट्रीय समस्या का एक अंग है। यह केवल आंशिक रूप से सही है। अन्य पिछड़ा वर्गों को वंचित रखना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, यहाँ मूल प्रश्न सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का है और गरीबी तो केवल इनको पंगु बना देने वाले जाति पर आधारित इन प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। चूँकि ये प्रतिबंध हमारे सामाजिक ढाँचे में जुड़ चुके हैं इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए ढाँचे में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। देश के शासक वर्गों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के बोध के सम्बन्ध में किए गए परिवर्तन भी कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे।
*आरक्षण-*
(13.2) विशिष्ट शासक वर्ग के दृष्टिकोण में एक ऐसे ही परिवर्तन का सम्बन्ध का अन्य पिछड़ा वर्गो के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था का किया जाना हैं। सामान्यतया यह तर्क दिया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्गों की बहुत बड़ी जनसंख्या (52%) को देखते हुए, आरक्षित रिक्तियों पर प्रत्येक वर्ष कुछ हजार अन्य पिछड़े वर्ग की भरती से उनकी आम स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, आरक्षित रिक्तियों में बड़े अनुपात में कर्मचारियों को रख लेने से सरकारी सेवाओं के स्तर और कार्यकुशलता को काफी नुकसान पहुँचेगा। यह भी कहा जाता है कि ऐसे आरक्षणों का लाभ अन्य पिछड़ा वर्गों के उन व्यक्तियों द्वारा उठाया जायेगा जो कि पहले ही सम्पन्न हैं और वास्तविक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति निस्सहाय ही रह जायेंगे। इस विचार के विरुद्ध एक दूसरा तर्क यह दिया गया है कि बड़े पैमाने पर आरक्षण नीति से उन योग्य उम्मीदवारों के मन गहरी ईर्ष्या से भर जायेंगे जिसका सेवाओं में प्रवेश इसके फलस्वरूप रोक दिया जायगा।
(13.3) उक्त सभी तर्क पूर्ण रूप से युक्तियुक्त विवेचन पर आधारित है। किन्तु ये तर्क भी उन विशिष्ट प्रशासकों द्वारा दिए गए हैं, जो अपनी सुविधाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए, ऐसे सभी तर्क किसी एकपक्षीय दृष्टिकोण पर आधारित है। इसी प्रकार कुछ तात्कालिक महत्व वाले क्षेत्रों पर विचार करते समय इसी प्रकार के संकेतों द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली अधिक बड़ी समस्यायों की उपेक्षा की जाती है।
(13.4) हमारा यह दावा कभी नहीं रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को कुछ हजार नौकरियाँ दे देने भर से हम भारतीय जनसंख्या के 52% को उन्नत करने में समर्थ हो जायेंगे। लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सामाजिक पिछड़ेपन के विरुद्ध लड़ाई पिछड़े लोगों के मन में लड़ी जानी है। भारत में, सरकारी सेवा को हमेशा प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया है। सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर हम उन्हें इस देश के शासन में शामिल होने का अनुभव कराते हैं। जब कोई पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार एक कलैक्टर या पुलिस अधीक्षक बन जाता है, तो उस पद से प्राप्त होने वाले फायदे केवल उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन इस बात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है कि उक्त पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार का समूचा समुदाय अपने आपको सामाजिक रूप से उन्नत महसूस करने लगता है। सामान्यतः जब कोई स्थाई लाभ समुदाय को नहीं मिलते हैं, तब यह भावना कि “शक्ति के गलियारे” में अब उनका ” अपना आदमी” है, एक साहसबर्द्धक के रूप में कार्य करती है।
(13.5) किसी लोकतांत्रिक ढाँचे में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को, इस देश के शासन में भाग लेने के लिए, वैध अधिकार और आकांक्षायें प्राप्त
हैं। कोई भी स्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनसख्या के लगभग 52% उक्त अधिकार से वंचित
हो जाते हैं, तो उसमें शीघ्र सुधार करने की जरूरत है।
(13.6) आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर ले लेने से सरकारी सेवाओं के स्तर के गिरने की आशंका भी केवल एक सीमा तक न्यायोचित लगती है। किन्तु क्या यह मानना संभव है कि योग्यता के आधार पर चुने गए सभी उम्मीदार ईमानदार, कुशल, परिश्रमी और निष्ठावान साबित होते हैं? इस समय सभी सरकारी सेवाओं में शीर्ष पदों पर मुख्यतया खुली प्रतियोगिता द्वारा लिए गए उम्मीदवार हैं, और यदि यह निष्पादन हमारी नौकरशाही का कोई सूचक है, तो इसने वास्तव में अपने आपको सही अर्थों में गौरवान्वित नहीं किया हैं तथापि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरक्षित पदों पर चुने गए उम्मीदवार अच्छा कर पायेंगे। लेकिन इस बात की संभावना है कि अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक बाधाओं के कारण वे सामान्यतया निष्पक्ष और सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत, उनके पास समाज के पिछड़ा वर्गो की कठिनाईयों और समस्यायों की प्रत्यक्ष जानकारी होने का बहुत लाभ होगा। सर्वोच्च स्तर पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए यह कम महत्व की बात नहीं है।
(13.7) निस्संदेह यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के अधिकांश लाभों को पिछड़ा समुदायों के अधिक उन्नत वर्गों द्वारा समेट लिया जायगा । किन्तु क्या यह एक सार्वभौम तथ्य नहीं है? धर्मतंत्रीय व्यवस्था के साथ-साथ सभी सुधारवादी उपायों का प्रभाव धीमा होता है और सामाजिक सुधारों की कोई मात्रा नहीं होती। चूँकि मानव प्रवृति उत्सुकता प्रधान होती है, इसलिए वर्गहीन समाज में भी उन्नत एक ‘नया वर्ग’ बन जाता है। आरक्षण की मुख्य विशेषता यह नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्गों में इसके द्वारा समतावाद आ जायगा, जब कि शेष भारतीय समाज सभी प्रकार की असमानताओं से घिरा हुआ है। किन्तु आरक्षण के द्वारा सेवाओं पर से उच्च जातियों की जकड़ निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी और आम तौर पर अन्य पिछड़ा वर्गों में अपने देश के कार्य संचालन में भाग लेने की भावना जागृत होगी।
(13.8) वास्तव में यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण किये जाने से अन्यों के मन में काफी ईर्ष्या पैदा होगी। लेकिन क्या केवल इस ईर्ष्या को सामाजिक सुधार के विरुद्ध नैतिक निषेधाधिकार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर काफी ईर्ष्या हुई थीं, सभी गोरों के मन ईर्ष्या पैदा होती है जब काले लोग दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हैं। जब कि उच्च जातियाँ जो कि देश की जनसंख्या के 20% से भी कम हैं, शेष अन्यों के साथ सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय करती रही है, इससे निम्न जातियों के मन में भी बहुत ईर्ष्या हुई होगी। किन्तु अब जबकि निम्नजातियाँ शक्ति और प्रतिष्ठा के राष्ट्रीय अंश में से थोड़े से हिस्से की मांग कर रही हैं तो यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे विशिष्ट शासकों के मन में ईर्ष्या होगी। पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के विरुद्ध दिए गए सभी निरर्थक तर्कों में कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो ईर्ष्या की स्थिति होने को साबित करता है।
(13.9) वास्तव में हिन्दू समाज ने हमेशा से आरक्षण की एक बहुत ही कठोर योजना चलाई है। जिसे जातीयता के जरिये आंतरिक रूप दिया गया था। आरक्षण के जाति नियमों का उल्लंघन करने के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा खोया और शम्बूक अपनी गर्दन। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध मौजूदा आक्रोश स्वयं सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, परन्तु लाभ पाने वालों के लिए धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि अब वे इन अवसरों की मांग कर रहे हैं जिन पर ऊँची जातियों ने अपना एकाधिकार जमाया हुआ है।
*आरक्षण की मात्रा और योजना*
(13.10) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ देश की जनसंख्या का 22.5% है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी सेवाओं में और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में उनके लिए 22.5% का यथानुपात आरक्षण किया गया है। राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।
(13.11) जैसा कि पिछले अध्याय (पैरा 12.13 में बताया गया था कि हिन्दू और गैर हिन्दू दोनों को मिलाकर अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% है। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीन 52% पद उनके लिए आरक्षित होने चाहिए। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में निर्धारित कानून के विरुद्ध जाता है, जिसमें यह माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16 (4) के अन्तर्गत आरक्षण की मात्रा 50% से कम होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण उस संख्या तक सीमित रखना होगा, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 22.5% आरक्षण जोड़ने से यह 50% से कम रहे। इस कानूनी अड़चन के कारण, आयोग केवल 27% आरक्षण की सिफारिश करता है जबकि उनकी जनसंख्या उक्त संख्या से लगभग दुगुनी है।
(13.12) वे राज्य, जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% से अधिक आरक्षण किया हुआ है, उन पर इस सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(13.13) आरक्षण की मात्रा के सम्बन्ध में उपर्युक्त सामान्य सिफारिश के साथ, आयोग अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की निम्नलिखित समय योजना का प्रस्ताव रखता है-
(1) *खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को उनके 27% के आरक्षण कोटा के साथ समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।*
(2) उपर्युक्त आरक्षण को सभी स्तरों पर पदोन्नति (Promotion) कोटा में भी ग्राह्य बनाया जाना चाहिए।
(3) न भरे गए आरक्षण कोटा को तीन साल की अवधि तक के लिए जारी रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात अनारक्षित किया जाय।
(4) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा में छूट उसी प्रकार से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए जिस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में दी जाती है।
(5) पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिस प्रकार से वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।
(13.14) आरक्षण की उपर्युक्त योजना को, पूर्ण रूप में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी भर्तियों में भी लागू किया जाना चाहिए।
(13.15) सरकार से किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में भी उपर्युक्त के आधार पर कार्मिकों की भर्ती करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
(13.16) सभी विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कॉलेजों को भी आरक्षण की उपर्युक्त योजना के बारे में लिखा जाना चाहिए।
(13.17) इन सिफारिशों को समुचित रूप से प्रभावी बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वर्तमान अधिनियमों, कानूनों,कार्यविधियों आदि को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त ससांविधिक प्रावधान उस सीमा तक करने चाहिए जब तक कि वे इन सिफारिशों के अनुरूप न बन जाए।
*शैक्षणिक रियायतें-*
(13.18) हमारी शैक्षणिक प्रणाली का स्वरूप एक विशिष्ट प्रकार का है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी अपव्यय होता है और यह किसी अधिक जन-संख्या वाले तथा विकासशील देश की आवश्यकताओं के मुताबिक कम उपयुक्त है। यह ब्रिटिश शासन की देन है जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी निन्दा की गई थी, किन्तु अभी भी इसमें कोई, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि यह पिछड़ा वर्गों की आवश्यकताओं के लिए कम से कम उपयुक्त है, तथापि उन्हें अन्यों के साथ तेज होड़ लगानी पड़ती है क्योंकि इसके सिवाय उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। चूंकि, ‘शिक्षा सुधार’ इस आयोग के विचारार्थ विषय के अन्तर्गत नहीं है, इसलिए हमें उक्त मार्ग पर पैर फूँक फूँक कर चलना पड़ता है और वर्तमान ठाँचे के अन्तर्गत छोटे-छोटे उपायों का ही सुझाव देने के लिए विवश होना पड़ता है।
(13.19) विभिन्न राज्य सरकारें अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों (अध्याय 9, पैरा 9-30-9-33) को ट्यूशन फीस से छूट, किताबों और वस्त्रों की मुफ्त पूर्ति, दोपहर का भोजन, विशेष छात्रावास सुविधाएँ, बजीफा आदि जैसी अनेक शैक्षणिक रियायतें दे रही हैं। ये रियायतें ठीक हैं,जब तक वे दी जाती हैं। किन्तु वे अधिक पर्याप्त नहीं हैं। अपेक्षित यह है कि शायद अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर देना ही पर्याप्त नहीं है अपितु वास्तविक तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के लिए उचित वातावरण बनाने तथा प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत योजनाएँ बनाई जाएं।
(13.20) यह सब जानते हैं कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के बच्चे अनियमित और उदासीन छात्र
होते हैं और उनकी बीच में शिक्षा छोड़ देने की दर बहुत अधिक होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं- पहला, ये बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अति अनुपयुक्त वातावरण में पलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने सम्बन्धी प्रेरणा की आमतौर पर कमी रहती है। दूसरे अधिकांश ये बच्चे बहुत ही गरीब घरों के होते हैं और उनके माता पिता उन पर बहुत ही छोटी आयु से छोटा-मोटा काम-काज करने के लिए दबाव डालने लग जाते हैं।
(13.21) सांस्कृतिक वातावरण को उन्नत बनाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। इन बच्चों को कृत्रिम रूप से ऊँचे किए गए वातावरण में रखने का काम इस समय देश में उपलब्ध साधनों से सम्भव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि इस समस्या को दो मोर्चों पर सीमित और चुनींदा आधार पर हल किया जाए।
(13.22) पहला अन्य पिछड़ा वर्गों की अत्यधिक घनी आबादी वाले चुने गए पोकेट्स में भी प्रौढ़ शिक्षा के गहन तथा समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। यह मूलतः एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण है, क्योंकि पर्याप्त रूप से प्रेरित माता-पिता ही अपने बच्चों को पढ़ाने में वास्तविक रूचि दिखाएंगे, दूसरे इन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए वास्तविक पढ़ाई के लिए विशेष प्ररेणा दायक वातावरण उपलब्ध करने की दृष्टि से आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। गरीब और पिछड़े घरों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए इन स्कूलों में सभी सुविधाएँ जिनमें खान-पान, रहन-सहन शामिल है, मुफ्त उपलब्ध करानी होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त सुविधाओं वाले पृथक सरकारी छात्रावास स्थापित करना उचित दिशा में सही कदम होगा।
(13.23) इन दोनों मोर्चों पर शुरूआत सीमित पैमाने तथा चुनींदा आधार पर करनी होगी। किन्तु इन गतिविधियों के क्षेत्र को, साधनों के अनुरूप तीव्रता से बढ़ाया जाना चाहिए। चुनींदा आधार पर शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और आवासीय स्कूलों से समूचे समुदाय की चेतना को बढ़ावा मिलेगा और उसका बहुमुखी प्रभाव भी काफी होगा। जहाँ कई राज्यों द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अनेक तदर्थं रियायतें दी जा रही हैं, वहीं अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों की उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक विशाल योजना के रूप में इन सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए कुछेक गम्भीर प्रयास भी किए गए हैं।
(13.25) यह भी स्पष्ट है कि यदि उपर्युक्त सभी सुविधाएँ अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी जाएँ, तो भी वे तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले के लिए अन्यों के साथ समान से प्रतियोगिता में नहीं आ सकेंगे। इसको दृष्टि में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत आएगा और आरक्षण का कोटा सरकारी सेवाओं के समान अर्थात् 27% होना चाहिए। उन राज्यों पर, जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए पहले से ही 27% से अधिक सीटों के लिए आरक्षण किया हुआ है, इस सिफारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(13.26) तथापि, आरक्षण के प्रावधान को कार्यान्वित करते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवार जिन्हें आरक्षित कोटा में
प्रवेश दिया जाता है, वे उच्च अध्ययन का पूरा लाभ उठा सकें। आमतौर पर यह देखा गया है कि ये अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र निर्धन व गैर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं, इसलिए वे अन्य छात्रों की बराबरी नहीं कर पाते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि ऐसे सभी छात्रों के लिए हमारे तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों में विशेष कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सम्बन्धित प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिए कि उनका कार्य केवल उम्मीदवारों को आरक्षित कोटा में विभिन्न स्थानों में दाखिला दे देने से समाप्त नहीं हो जाता है। बल्कि उनका काम तो वास्तव में इसके बाद शुरू होता है। जब तक इन छात्रों को विशेष कोचिंग सहायता देने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जायगी तब तक ये युवक न केवल निराश और कुंठित रहेंगे बल्कि देश साधनहीन और घटिया इंजिनियरों, डाक्टरों तथा अन्य व्यावसायियों से भी भर जायगा।
*वित्तीय सहायता-*
(13.27) औद्योगीकरण के फलस्वरूप पुश्तैनी व्यवसाय अपनाने वाले व्यावसायिक समुदायों को काफी हानि पहुँची है। मशीनी उत्पादन तथा कृत्रिम सामग्री की शुरूआत ने ग्रामीण कुम्हार, तेल निकालने वाले लोहार, बढ़ई, मछुआरे आदि को उनके जीवन यापन के पुश्तैनी साधनों से वंचित कर दिया और गांवों में इन वर्गों की निर्धनता के बारे में सब भलीभाँति जानते हैं।
(13.28) इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि गाँव के उन व्यवसायिक समुदायों के लोगों को समुचित वित्त तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाय, जो अपने स्वयं के लघु उद्योग लगाना चाहते हैं। इसी प्रकार की सहायता अन्य
पिछड़े वर्गों के उन होनहार उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए जिन्होंने विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
(13.29) वास्तव में, बहुत सी राज्य सरकारों ने लघु तथा मझोले उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय तथा तकनीकी एजेंसियां बनायी हैं। परन्तु यह भलिभांति विदित है कि समुदाय के केवल अधिक प्रभाव शाली व्यक्ति ही इन एजेंसियों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इसको दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु पृथक वित्तीय संस्थायें स्थापित की जाएँ। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से पहले ही वित्तीय निगम आदि स्थापित किए हुए हैं।
(13.30) व्यावसायिक ग्रुपों की सहकारी समितियाँ भी बहुत सहायक होंगी। इसकी पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि इन समितियों के सभी पदाधिकारीगण और सदस्य पैतृक व्यावसायिक ग्रुपों से सम्बन्धित होने चाहिए और बाहरी लोगों को इन समितियों में घुसकर उनका शोषण नहीं करने देना चाहिए।
(13.31) देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन में अन्य पिछड़े वर्गो का हिस्सा नगण्य है और अंशत: उनके न्यूनतम आय स्तर का द्योतक है। पिछड़े वर्गों के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों में व्यापारिक तथा औद्योगिक उद्यमों को विकसित करने के लिए पृथक वित्तीय तथा तकनीकी संस्थाओं का एक जाल बिछाने हेतु सलाह और बढ़ावा दिया जाए। *संरचना सम्बन्धी परिवर्तन*
(13.32) सरकारी रोजगार तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सभी सम्भव वित्तीय सहायता भी उस समय तक बहुत ही थोड़ी समझी जाएगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या को उसकी जड़ से न सुलझाया जाए। छोटे भूमिधारी, काश्तकार, किसान मजदूर, असहाय ग्रामीण कारीगर, अकुशल मजदूर आदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं। ‘सामाजिक परम्पराओं के अलावा, उच्च किसान वर्ग गरीब किसानों को रूपया उधार देकर पट्टे पर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े देकर घरों के लिए तथा रहने के लिए भूमि देकर और अनौपचारिक बेगार करा कर उन पर शासन करता है। चूँकि सरकारी पदाधिकारी अधिकांश उच्च किसान वर्ग से होते हैं इसलिए पदाधिकारियों तथा उच्च किसान वर्गों के बीच वर्ग तथा जाति सम्बन्ध अटूट रहते हैं। यह सामाजिक तथा राजनीतिक सन्तुलन उच्च किसान वर्ग के पक्ष में कर देता है और दूसरों पर उनका प्रभुत्व रखने में उनकी सहायता करता है।”
(13.33) उपर्युक्त परिस्थिति का निश्चित परिणाम यह होता है कि उनकी अधिक संख्या होने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग उच्च जातियों तथा सम्पन्न कृषक वर्ग का मानसिक तथा शारीरिक रूप से बन्धक बना रहता है। देश की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या होने के बावजूद अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग एक बहुत ही थोड़ी सी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर पाए हैं, जबकि वयस्क मताधिकार पिछले तीन दशकों से अधिक समय से पूर्व शुरू किया गया था। उत्पादन के साधनों पर अपने एकाधिकार से उच्च जातियां पिछड़े वर्ग को अपनी इच्छाओं के विरूद्ध कार्य करने के लिए किसी न किसी तरह बाध्य कर देती हैं।
*मण्डल कमीशन का आधार क्या हो*
हमारे इतिहास के किस दौर में आरक्षण का चलन नहीं था? हमारी जाति व्यवस्था ही जन्म से आरक्षण की मनुष्य द्वारा सोची गई सबसे पुरानी व्यवस्था है। सिर्फ ब्राह्मणों को ही वैदिक ज्ञान का अधिकार था, सिर्फ क्षत्रिय ही हथियार उठा सकते थे, शम्बूक नामक शूद्र जब उत्तराखण्ड के जंगलों में गहन ध्यान में डूबा था तो मर्यादा पुरूषोत्तम राम ने उसका सिर उतार लिया था, क्योंकि उसने ऊँची जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया था।जातिवाद के कारण ही निषाद पुत्र एकलव्य का अँगूठा कटवा लिया गया था।ये दो घटनाएं मनुवादी व्यवस्था व वंचित वर्ग के प्रतिभा हनन का षडयंत्र था।
मण्डल आयोग के सचिव के नाते मैं देश भर के सैकड़ों जातीय संगठनों से मिला और उस अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा और आगे बढ़ने के अवसर का पासपोर्ट तो जाति ही है। ऊँची जाति वाले आज भी जिस प्रकार नीची जाति की औरतों की इज्जत से खेलते हैं, जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं, नीची जातियों की जमीन पर मालिक मानने से इन्कार करते हैं और हर संभव तरीके से उनका अपमान करते हैं। वह सब देखे वगैर शहरी बौद्धिकों की समझ में नहीं आ सकता है। शादी व्याह की बातें दूर रही, आज भी गिनती के ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर मिलेंगे जो नीची जाति वालों के साथ बैठकर खाने को तैयार हो ।
इस आयोग के अध्यक्ष विन्देश्वरी प्रसाद मंडल, जो जाति के ग्वाला या यादव थे, बड़ी भावुकता से सुनाया करते थे कि कैसे जब वे पहली बार स्कूल गये तो उनके शिक्षक ने उन्हें ऊँची जाति वाले लड़कों के साथ बैठने नहीं दिया और यह तब जब उनके पिता उस इलाके के सबसे बड़े भूमिवान/जमीदार थे।
-एस. एस. गिल
सचिव-मण्डल कमीशन
मेरा कहना यह नहीं है कि (दूपिजा) दूसरी पिछड़ी जातियों को इतिहास की भूल सुधारने के लिए जबाबी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जातिगत आरक्षण के नाम से ही जो आग बबूला हो उठते हैं, उन्हें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जातीय आध र पर आरक्षण की कल्पना कहीं चंडूल खाने से उठाकर नहीं लायी गई है। इसकी जड़ें इस समाज में गहरी धँसी हुई है जिसने 3000 सालों से भी ज्यादा से इसका बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया है, उसने धार्मिक सिद्धान्तों के नैतिक आतंक से नीची जातियों के अन्तरतम में हीनता की भावना भर दी है और उनकी मनोभूमिका ही पंगु बना दी है।
कर्पूरी ठाकुर
(भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार)
यह जोर-जोर से नारा लगाया जाता है कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए न कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, इस नारे के पीछे बेईमानी और चालबाजी है। सचमुच में यह अनुसूचित जाति विरोध, जनजाति विरोध, पिछड़ा विरोध एवं संविधान विरोध है। अपने देश में हजारो वर्षों से छुआछूत, ऊँच-नीच बड़ा-छोटा, सम्मान-अपमान का जो भेदभाव रहा है, क्या उसका आधार आर्थिक है? कदापि नहीं। उसका आधार तो शत प्रतिशत सामाजिक है, वह तो विषमता मूलक जाति व्यवस्था का स्पष्ट परिणाम है।
प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन भारत में शम्बूक वध का दृष्टान्त, एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य द्वारा दक्षिणा में कटवा लेने का उदाहरण, शिवाजी के राज्यभिषेक में दक्षिण भारत के ब्राह्मणों द्वारा प्रचण्ड विरोध का इतिहास, काशी में बाबू जगजीवन राम द्वारा सम्पूर्णानन्द जी की प्रतिमा का अनावरण के उपरान्त कट्टरपंथी ब्राह्मणों द्वारा गंगाजल से मूर्ति का प्रक्षालन, डा.अम्बेडकर के नाम पर औरंगाबाद में मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के नामकरण का विरोध, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के मंदिर प्रवेश का विरोध, वर्षो पूर्व शूद्रों द्वारा यज्ञोपवीत धारण का विरोध, शूद्रों और पिछड़ों पर अमानुषिक अन्याय-अत्याचार तथा उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक हत्यायें, और उनकी बहू बेटियों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक बलात्कार की घटनायें, क्या किसी आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित हैं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं ।
जो आर्थिक आधार की थोथी दलील देता है, वह या तो भारतीय समाज की वस्तु स्थिति (हकीकत) से पूर्ण अनभिज्ञ है या सत्यता पर पर्दा डालने वाला है या स्वार्थी और बेईमान है या राष्टहंता है, समाजहंता है। राष्ट्र एवं समाज रूपी सम्पूर्ण शरीर के सम्पूर्ण विकास का सम्पूर्ण विरोधी ही इस प्रकार की दलील दे सकता है।’
*-एस.एम. जोशी*
(एक प्रख्यात समाजशास्त्री)
प्रजातंत्र को दृढ़मूल(मजबूत) करने के लिए मण्डल आयोग के सुझाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे सुझाव केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं, अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए हैं, उसका स्वरूप राष्ट्रीय है। यदि प्रजातंत्र चाहिए तो सामाजिक तथा आर्थिक समता शीघ्रताशीघ्र प्रस्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने देश में आर्थिक विषमता है, उससे भी अधिक सर्वमान्य को पीड़ा देने वाली सामाजिक विषमता है।
*हिन्दू समाज का कलंक*
*वर्ण और जाति पर आधारित विषमता मूलक तथा अपमान जनक सामाजिक व्यवस्था*
भारतीय सामाजिक पद्धति में घोर असमानता है। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से प्राचीन जाति प्रथा पर आधारित है। आज भी जन्मजात असमानता विद्यमान है। जन संख्या के एक बहुत बड़े भाग जो आज भी अछूत हैं, शूद्र तथा बैकवर्ड समझा जाता है और उन्हें नफरत की नजर से देखा जाता है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी हिन्दुओं का जीवन हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार आज भी चलाने की कुचेष्टा की जा रही है। इनके अनुसार विभिन्न पिछड़ी जातियों या शूद्रों के अधिकार और कर्तव्य का अलग-अलग निर्धारण किया गया है जो विषमता, अपमान और शोषण पर आधारित है। अनेक अमानुषिक प्रथाओं और धर्मोपदेशों ने हिन्दू जाति के बहुलांश के जीवन को घोर यातनापूर्ण तथा नारकीय बना दिया है। हिन्दूधर्म में जन्म पर आधारित जाति प्रथा एक अत्यंत ही सांघातिक तथा अमानवीय सिद्धान्त है।
भारत में सामाजिक संस्तरण/स्तरीकरण(social status/stratification) अति प्राचीन काल से वर्ण पर आधारित था। जब वर्णों से जाति व्यवस्था का विकास हुआ तो जाति ही संस्तरण (status) का आधार बन गया। पश्चिमी देशों में वर्ग ही सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण का आधार है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। जब तक इस देश में विषमता मूलक पीड़ा दायिनी जाति प्रथा कायम रहेगी, तब तक वर्ग की बात चलाना या आरक्षण आदि में आर्थिक आधार की बात करना एक फिजूल की बकवास होगी।
एक व्यक्ति परिश्रम करके धनी बन सकता है और दूसरी ओर एक धनी व्यक्ति दीवाला निकलने पर गरीब हो सकता है। लेकिन निम्न या पिछड़ी जाति का व्यक्ति धनी होने के बाद भी अपनी निम्नता और शूद्र कहे जाने के कलंक से बरी नहीं हो सकता। इस देश में आर्थिक विषमता से भी बढ़ चढ़ कर दिल को कचोटने, काटने और दिमाग को झकझोरने वाली पीड़ादायिनी सामाजिक विषमता है।
‘विगत 3000 वर्षों से जाति प्रथा की जकड़न में फँसा हिन्दू समाज आज भी इससे मुक्त नहीं हो सकता है बल्कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले में धर्म और धार्मिक ग्रन्थों की खासी भूमिका रही है। ब्राह्मणबाद ने गैर सवर्णों का कैसा विकट शोषण किया है, इसे हम आज भी देख रहे हैं। अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में कानूनी जुर्म करार दिये जाने के बाद भी शूद्रों को सवर्णों के कुंए से पानी भरने की इजाजत नहीं मिलती, उन्हें मंदिरों के द्वार से भगा दिया जाता है, वे आज भी बांटी गई जमीनों से बेदखल किये जाते हैं और यदि उनका दूल्हा घोड़ी पर बैठकर सवर्णों की गली से गुजर जाय तो उसे वहीं उतार कर मारा पीटा जाता है। आज भी कोई शूद्र ब्राह्मण ,भूमिहार या ठाकुर के दरवाजे के सामने से छाता लगाकर नहीं गुजर सकता।” चमरवा, दुसाधवा, गोआरवा, शूदरवा, तेलिया, तमोलिया, तुराहवां, मलहवा, बिनवा, केवटवा, धिमरा, कहरवा, गोड़वा, धोबिया,नउआ, पसिया,धरकरवा,बाँसफोरवा, कलवरवा,बरिया, गोंड़वा,कछिया,
मलिया,कोइरिया,मुसहरवा और नन्हजतिया आदि सामाजिक अपमान से भरी दिल को कचोटने वाली शब्दावलियाँ किसी आर्थिक आधार पर नहीं है।
अगर गैर सवर्ण पिछड़ा, दलित समाज का व्यक्ति विद्यालय में पढ़ने जाता था तो सवर्ण ब्राह्मण, भूमिहार व राजपूत शिक्षकों द्वारा मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाया जाता था, उसे इस तरह प्रताड़ित व अपमानित किया जाता था कि वह विद्यालय जाने का फिर नाम न ले सके।इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सवर्ण भविष्य को देखकर कार्य करता था, उसे आभास था कि यदि पिछड़े, शूद्र पढ़ लिख लेंगे तो उनमें व उनकी संतानों में सम्मान, स्वाभिमान व अधिकार की भूख जागेगी तो तुच्छ जातिवादी शिक्षक इन्हें मानसिक विकलांगता का शिकार बनाये रखने के लिए तरह-तरह से आघातित करते थे। मुझे जाति व्यवस्था के दंश का कटु अनुभव है। जो मल्लाह, चमार के लड़के विद्यालय में पढ़ने आते थे तो सवर्ण शिक्षक मुर्गा बनाकर पीठ पर ईंट रख देते थे, जूता पहने पैरों से मारते थे और कहते थे कि जाओ कछुवा, सिधरी, मछली पकड़ो कि पढ़ने आये हो डी.एम. कलेक्टर बनोगे। सवर्ण शिक्षकों के घृणित कारनामों, दुर्व्यवहार व मानसिक पीड़ादायक कुकृत्यों से पिछड़ा, दलित बच्चा टूट जाता था, डर के मारे स्कूल नहीं जाता था, पर जो लात जूते खाकर व अपमान सहकर अड़ा रहा उसमें से कुछ आगे बढ़ गये। मुझे भी जाति व्यवस्था आधारित दोषों का कटु अनुभव है। जिन्हें मैं स्वयं झेला हूँ, उसका शिकार हुआ हूँ।
*- लौटन राम निषाद*
(लेखक सामाजिक न्यायचिन्तक व भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)
*जो कोई भी अपने समय के इतिहास को लिखता है, उसे अपनी सभी कही और अनकहीं बातों के लिए लोगों का अप्रीतिभाजन बनना पड़ता है, लेकिन जो सत्यता और स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं, वे इन बाधाओं से हतोत्साहित नहीं होते हैं और निन्दा-प्रशंसा से अप्रभावित रहकर निर्भीकता से अपनी कलम चलाते रहते हैं। (वॉल्टेयर)*